
फल पौधों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन
(सभी तस्वीरें- हलधर)एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन एक ऐसी विधि है जिसमें कार्बनिक, अकार्बनिक और जैविक स्रोतों के मिश्रित उपयोग द्वारा पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करवाये जाते है। इसके उद्देश्य उर्वरक उपयोग क्षमता को अधिक करना, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को बढ़ाना आदि से सम्बन्धित रहते है। ताकि, लंबे समय तक स्थाई कृषि द्वारा अधिक उत्पादन लिया जा सके। एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन, तकनीकी रूप से परिपूर्ण, आर्थिक रूप से आकर्षक, व्यावहारिक रूप से सम्भव और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होना अनिवार्य है।
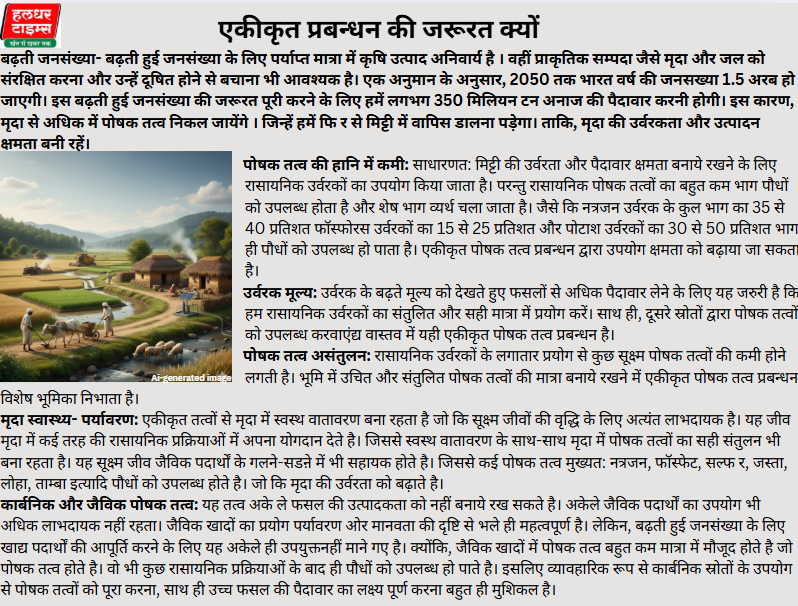
पोषक तत्वों के मुख्य स्रोत
> यूरिया नत्रजन (46प्रतिशत)
> सिंगल सुपर फ ास्फेट (16 प्रतिशत)
> म्यूरेट ऑफ पोटाश (60प्रतिशत)
> कैन नत्रजन (25प्रतिशत)
> राक फ ास्फेट (25प्रतिशत)
जैविक खाद: जैविक पदार्थों में गली सड़ी पत्तियां, टहनियां, फल, फूल और जानवरों के मलमूत्र इत्यादि सम्मलित होते है। सभी प्रकार के जैविक व्यर्थ जैसे फसलों के अवशेष, खरपतवार इत्यादि भी जैविक पदार्थों के प्रकार है। इन पदार्थों को खेतों में डालने से पहले अच्छी तरह से गलाया व सड़ाया जाता ही, जिसे कम्पोस्टिंग कहते है।
समृद्ध खाद बनाने की विधि
सर्वप्रथम (3:1:1 मीटर) की न्यूनतम आयतन का गड्ढा खोदें। गड्ढे का आकार उपलब्ध भूमि के अनुसार बदला भी जा सकता है। उपलब्ध जैविक अवशेषों जैसे खरपतवार, घासफूस, वृक्षों के पत्ते तथा फसलों आदि को बारीक काट लें। यूरिया (2.8 किलोग्राम) रॉक फॉस्फोरस (5.6 किलोग्राम) ताजा गाय का गोबर (180 किलोग्राम), सिचाई पानी, मिट्टी आदि तैयार रखें।ये मात्रा उपरोक्त आयात के गड्ढे के लिए पर्याप्त है। लगभग 10 किलो गोबर का 10-15 लीटर पानी में घोल बनाएं और पहली परत के रूप में डाल दें। गड्ढे में कटे कार्बनिक अवशेष तथा 200 ग्राम यूरिया 400 ग्राम रॉक फॉस्फोरस10 किलो ताजा गोबर 10-15 लीटर पानी का घोल बना के 4.5 इंच की परत बना दें। इस प्रकार गड्ढे में गोबर व जीवांश क्रमश: डालें। जब गड्ढा भर जाये तो इसे ऊपर से घासफूस से ढक दें। यह एक महीने के लिए छोड़ दें। इसे खोलें और अच्छी तरह मिलाएं तथा 50-60 लीटर पानी डालें और 15-20 दिन इसी रूप में रखें। जिसके उपरांत, समृद्ध खाद तैयार हो जाएगी। एक अच्छी जैविक खाद वही होती है जो गहरी भूरे रंग के साथ-साथ भुरभुरी प्रकृति की हो।
हरित खाद: हरित खाद के लिए कुछ खास फसलों को उगाया जाता है जिन्है। परिपक्व होने से पहले ही काट दिया जाता है और मृदा में मिलाया जाता है। एक दो महीने में सड़ कर जैविक खाद बना देती है।
कन्सेन्ट्रेटीड जैविक पदार्थ: जैविक पदार्थों को कुछ विशेष प्रक्रियाओं से गुजारने पर कन्सेन्ट्रेटीड जैविक पदार्थ बनते है। जिन्है जैविक खादों के रूप में उपयोग किया जाता है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा साधारण जैविक पदार्थों से अधिक होती है। इस श्रेणी में मुख्यत: सूखी मछली का चूरा, हड्डियों का चूर्ण, चोकर और खली शामिल है।
फलीदार पौधे लगाना: खेतों के आस-पास फलीदार पौधे लगाना भी एकीकृत पोषक तत्व प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। इन पौधों की जड़ों में गाठें होती है। जिनमें राईजोबियम बैक्टीरिया होते है। इस बैक्टीरिया में वातावरण से नत्रजन की स्थिर करने की क्षमता होती है जिसे पौधे उपयोग करते है। तथा अपनी नत्रजन की जरूरत को पूरा करते है। ल्यूसिनिया इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण पौधा है।
जीवांश खाद
इस श्रेणी में मुख्यत: नत्रजन स्थिरीकरण, फॉस्फोरस परिवर्तनशील सूक्ष्म जीव आते है। इन खादों में सूक्ष्म जीवों के सक्रिय एवं सुप्त कोशिकाएं होती है। बाजार में कई तरह की जीवांश खादें मौजूद है।
राईजोबियम बैक्टीरिया: यह एक सहजीवी नत्रजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव है। जो पौधों की जड़ों मने बनी विशेष गांठों में मौजूद होता है। यह बैक्टीरिया मृदा में 25-30 किलोग्राम हैक्टेयर की दर से नत्रजन मिलाता है।
ब्लू ग्रीन एल्गी (बी.जी.ए.): जैसे ऐनाबीना, नौस्टोक, ये जीव प्रतिवर्ष 20-30 किलोग्राम प्रतिशत हैक्टयर की दर से नत्रजन स्थिर करते है।
ऐजोटोबैक्टर: यह बैक्टीरिया मृदा में मौजूदा होता है जो 24-27 किलोग्राम हैक्टयर की दर से हर साल नत्रजन स्थिर करता है। इसके अलावा, यह सूक्ष्म जीव कई तरह के पादप वृद्धि हारमोन, विटामिन, कवकरोधी पदार्थ भी स्रावित करता है।
ऐजोस्पाईरिलम: यह हर साल मृदा में 15-20 किलोग्राम हैक्टयर की दर से नत्रजन मिलाता है।
माइकोराईजा: माइकोराईजा के प्रयोग से पौधों को पोषक तत्वों की होने वाली उपलब्धता बढ़ जाती है। इन पोषक तत्वों में मुख्यत: फॉस्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व आते है। इसके साथ-साथ जड़ क्षेत्र के आस-पास नत्रजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ जाती है।
फॉस्फोरस घुलनशील जीव : ये सूक्ष्म जीव मृदा में मौजूद अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करता है जिससे पौधों के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। उदाहरणत: रूयुडोमोनास, बैसीलस, एसपरजिलस जैसे सूक्ष्म जीव।